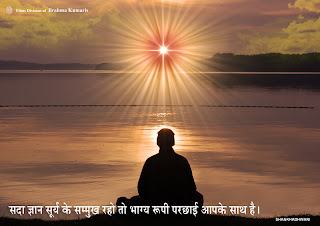Different exercises for different age groups and some special exercises for those who have Problems as per their need so get contact with experts and start exercises as per direction and get best result..........Do not follow T.V. or listen to any one sayings.
RJ Ramesh @RadioMadhuban | Inspiring Stories, Interviews & Ghazal Sessions Explore the inspiring journey of RJ Ramesh, the soulful voice behind Radio Madhuban 90.4 FM. Dive into heart-touching interviews, musical evenings, and stories from shows like 'Baatein Mulakatein' and 'Rubaroo'.
Saturday, August 3, 2013
Fitness Expert Karan`s Interview on Radio Madhuban
Different exercises for different age groups and some special exercises for those who have Problems as per their need so get contact with experts and start exercises as per direction and get best result..........Do not follow T.V. or listen to any one sayings.
Thursday, August 1, 2013
Monday, July 22, 2013
" गुरु पूर्णिमा "
गुरु पूर्णिमा / व्यास पूर्णिमा / मुड़िया पूनों आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की लाखों श्रद्धालु परिक्रमा देते हैं। बंगाली साधु सिर मुंडाकर परिक्रमा करते हैं क्योंकि आज के दिन सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हुआ था। ब्रज में इसे 'मुड़िया पूनों' कहा जाता है। आज का दिन गुरु–पूजा का दिन होता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो 'व्यास' नाम के कई विद्वान हुए हैं परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे। अत: वे हमारे 'आदिगुरु' हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने-अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण किया करते थे। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु कुटुम्ब में अपने से जो बड़ा है अर्थात माता-पिता, भाई-बहन आदि को भी गुरुतुल्य समझना चाहिए। गुरु पूर्णिमा जगत गुरु माने जाने वाले वेद व्यास को समर्पित है। माना जाता है कि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। वेदों के सार ब्रह्मसूत्र की रचना भी वेदव्यास ने आज ही के दिन की थी। वेद व्यास ने ही वेद ऋचाओं का संकलन कर वेदों को चार भागों में बांटा था। उन्होंने ही महाभारत, 18 पुराणों व 18 उप पुराणों की रचना की थी जिनमें भागवत पुराण जैसा अतुलनीय ग्रंथ भी शामिल है। ऐसे जगत गुरु के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा है।गुरु को गोविंद से भी ऊंचा कहा गया है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है- अंधकार या मूल अज्ञान और रु का का अर्थ किया गया है- उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन-शलाका से निवारण कर देता है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ‘गुरु’ कहा जाता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी। सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। ‘व्यास’ का शाब्दिक संपादक, वेदों का व्यास यानी विभाजन भी संपादन की श्रेणी में आता है। कथावाचक शब्द भी व्यास का पर्याय है। कथावाचन भी देश-काल-परिस्थिति के अनुरूप पौराणिक कथाओं का विश्लेषण भी संपादन है। भगवान वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों और उपपुराणों की रचना की। ऋषियों के बिखरे अनुभवों को समाजभोग्य बना कर व्यवस्थित किया।
व्रत और विधान.........
इस दिन (गुरु पूजा के दिन) प्रात:काल स्नान पूजा आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण कर गुरु के पास जाना चाहिए।
गुरु को ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर तथा धन भेंट करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। उसके हृदय का अज्ञानता का अन्धकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं और गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है।
गुरु पूर्णिमा पर व्यासजी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन-मनन करके उनके उपदेशों पर आचरण करना चाहिए।
इस दिन केवल गुरु (शिक्षक) ही नहीं, अपितु माता-पिता, बड़े भाई-बहन आदि की भी पूजा का विधान है।
इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए, अंधविश्वासों के आधार पर नहीं। गुरु पूजन का मन्त्र है-
'गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुदेव महेश्वर:।'
गुरु साक्षात्परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवे नम:।।
क्या करें गुरु पूर्णिमा के दिन .....
प्रातः घर की सफाई, स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ-सुथरे वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं।
घर के किसी पवित्र स्थान पर पटिए पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर 12-12 रेखाएं बनाकर व्यास-पीठ बनाना चाहिए।
फिर हमें 'गुरुपरंपरासिद्धयर्थं व्यासपूजां करिष्ये' मंत्र से पूजा का संकल्प लेना चाहिए।
तत्पश्चात दसों दिशाओं में अक्षत छोड़ना चाहिए।
फिर व्यासजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजी, गोविंद स्वामीजी और शंकराचार्यजी के नाम, मंत्र से पूजा का आवाहन करना चाहिए।
अब अपने गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करके उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देना चाहिए।
Tuesday, July 16, 2013
Harsh Tewari Experience Sharing with Radio madhuban
सादगी मैं एक अदा इतनी प्यारी लगी
आपकी दोस्ती हुमको सुबसे निराली लगी
यह ना टूटे कभी यही दुआ है
क्यू के यही इस दुनिया में हम को हमारी लगी..
आपकी दोस्ती हुमको सुबसे निराली लगी
यह ना टूटे कभी यही दुआ है
क्यू के यही इस दुनिया में हम को हमारी लगी..
Monday, July 15, 2013
जमशेद जी जीजाभाई - जीवन परिचय
जमशेद जी जीजाभाई - जीवन परिचय
जमशेद जी जीजाभाई का जन्म 15 जुलाई, 1883 ई. को एक गरीब परिवार में
मुंबई में हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। 12 वर्ष
की छोटी उम्र में अपने मामा के साथ पुरानी बोतलें बेचने के धंधे में लग गए थे।
कुछ दिन बाद ममेरी बहन से उनका विवाह भी हो गया। 1899 में माता-पिता का
देहांत हो जाने से परिवार का पूरा भार जमशेद जी के ऊपर आ गया।
उनमें बड़ी व्यवसाय-बुद्धि थी। व्यवहार से उन्होंने साधारण हिसाब रखना और
कामचलाऊ अंग्रेजी सीख ली थी। उन्होंने अपने व्यापार का भारत के बाहर विस्तार
किया। भाड़े के जहाजों में चीन के साथ वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने लगे।
20 वर्ष के थे तभी उन्होंने पहली चीन यात्रा की। कुल मिलाकर वे पांच बार चीन गए।
कभी ये यात्राएं खतरनाक भी सिद्ध हुईं। एक बार पुर्तग़ालियों ने इनका जहाज पकड़कर
लूट लिया और इन्हें केप ऑफ गुडहोप के पास छोड़ दिया था। किसी तरह मुंबई आकर
इन्होंने फिर अपने को संभाला और 1914 में अपना जहाज ख़रीदने के बाद जमशेद जी बेड़ा
बढ़ाने और निरंतर उन्नति की दिशा में बढ़ते गए।
महारानी विक्टोरिया द्वारा सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे।
सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहने वाले जीजाभाई ने महिलाओं की स्थिति सुधारने
तथा पारसी समाज की बुराइयां दूर करने के लिए भी अनेक क़दम उठाए।
योगदान---
दुर्भिक्ष सहायता, कुओं और बांधों का निर्माण, सड़कों और पुलों का निर्माण,
औषधालय स्थापना, शिक्षा-संस्थाएं, पशु-शालाएं, अनाथालय आदि सभी के लिए
उन्होंने धन दिया। उनकी आर्थिक सहायता से स्थापित संस्थाओं में प्रमुख हैं-
जे. जे. अस्पताल, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, पूना बांध और जल संस्थान।
‘मुंबई समाचार’ और ‘मुंबई टाइम्स’ (अब का टाइम्स ऑफ इंडिया)
जैसे पत्रों को भी सहायता मिली। अनुमानतः उस समय उन्होंने 30 लाख रुपये से अधिक का दान दिया था।
जमशेद जी जीजाभाई का जन्म 15 जुलाई, 1883 ई. को एक गरीब परिवार में
मुंबई में हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। 12 वर्ष
की छोटी उम्र में अपने मामा के साथ पुरानी बोतलें बेचने के धंधे में लग गए थे।
कुछ दिन बाद ममेरी बहन से उनका विवाह भी हो गया। 1899 में माता-पिता का
देहांत हो जाने से परिवार का पूरा भार जमशेद जी के ऊपर आ गया।
उनमें बड़ी व्यवसाय-बुद्धि थी। व्यवहार से उन्होंने साधारण हिसाब रखना और
कामचलाऊ अंग्रेजी सीख ली थी। उन्होंने अपने व्यापार का भारत के बाहर विस्तार
किया। भाड़े के जहाजों में चीन के साथ वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने लगे।
20 वर्ष के थे तभी उन्होंने पहली चीन यात्रा की। कुल मिलाकर वे पांच बार चीन गए।
कभी ये यात्राएं खतरनाक भी सिद्ध हुईं। एक बार पुर्तग़ालियों ने इनका जहाज पकड़कर
लूट लिया और इन्हें केप ऑफ गुडहोप के पास छोड़ दिया था। किसी तरह मुंबई आकर
इन्होंने फिर अपने को संभाला और 1914 में अपना जहाज ख़रीदने के बाद जमशेद जी बेड़ा
बढ़ाने और निरंतर उन्नति की दिशा में बढ़ते गए।
महारानी विक्टोरिया द्वारा सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे।
सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहने वाले जीजाभाई ने महिलाओं की स्थिति सुधारने
तथा पारसी समाज की बुराइयां दूर करने के लिए भी अनेक क़दम उठाए।
योगदान---
दुर्भिक्ष सहायता, कुओं और बांधों का निर्माण, सड़कों और पुलों का निर्माण,
औषधालय स्थापना, शिक्षा-संस्थाएं, पशु-शालाएं, अनाथालय आदि सभी के लिए
उन्होंने धन दिया। उनकी आर्थिक सहायता से स्थापित संस्थाओं में प्रमुख हैं-
जे. जे. अस्पताल, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, पूना बांध और जल संस्थान।
‘मुंबई समाचार’ और ‘मुंबई टाइम्स’ (अब का टाइम्स ऑफ इंडिया)
जैसे पत्रों को भी सहायता मिली। अनुमानतः उस समय उन्होंने 30 लाख रुपये से अधिक का दान दिया था।
Saturday, July 13, 2013
"जगन्नाथ रथयात्रा"
जगन्नाथ रथयात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महामहोत्सवों में सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रथयात्रा न केवल भारत अपितु विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी ख़ासी दिलचस्पी और आकर्षण का केंद्र बनती है। भगवान श्रीकृष्ण के अवतार 'जगन्नाथ' की रथयात्रा का पुण्य सौ यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली 'जगन्नाथ रथयात्रा उत्सव' के समय आस्था का जो विराट वैभव देखने को मिलता है, वह और कहीं दुर्लभ है। इस रथयात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुँचने का बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथयात्रा दस दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। देश-विदेश से लाखों लोग इस पर्व के साक्षी बनने हर वर्ष यहाँ आते हैं। भारत के चार पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्रीकृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा भी हैं।
वर्तमान रथयात्रा में जगन्नाथ को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है, उनमें विष्णु, कृष्ण और वामन और बुद्ध हैं। जगन्नाथ मंदिर में पूजा, आचार-व्यवहार, रीति-नीति और व्यवस्थाओं को शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्मावलम्बियों ने भी प्रभावित किया है। रथ का रूप श्रद्धा के रस से परिपूर्ण होता है। वह चलते समय शब्द करता है। उसमें धूप और अगरबत्ती की सुगंध होती है। इसे भक्तजनों का पवित्र स्पर्श प्राप्त होता है। रथ का निर्माण बुद्धि, चित्त और अहंकार से होता है, ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार रथयात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करता है और आत्मदृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रथयात्रा के समय रथ का संचालन आत्मा युक्त शरीर करता है जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है तो भी वह स्वयं संचालित नहीं होती, बल्कि उसे माया संचालित करती है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता बल्कि उसे खींचने के लिए लोक-शक्ति की आवश्यकता होती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार 'राजा इन्द्रद्युम्न' भगवान जगन्नाथ को 'शबर राजा' से यहां लेकर आये थे तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण कराया था जो बाद में नष्ट हो गया। इस मूल मंदिर का कब निर्माण हुआ और यह कब नष्ट हो गया इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। 'ययाति केशरी' ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था। वर्तमान 65 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल 'गंगदेव' तथा 'अनंग भीमदेव' ने कराया था। परंतु जगन्नाथ संप्रदाय वैदिक काल से लेकर अब तक मौजूद है।
भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के लिए रथों का निर्माण लकड़ियों से होता है। इसमें कोई भी कील या काँटा, किसी भी धातु का नहीं लगाया जाता। यह एक धार्मिक कार्य है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से 'वनजगा' महोत्सव से प्रारम्भ होता है तथा लकड़ियाँ चुनने का कार्य इसके पूर्व बसन्त पंचमी से शुरू हो जाता है। पुराने रथों की लकड़ियाँ भक्तजन श्रद्धापूर्वक ख़रीद लेते हैं और अपने–अपने घरों की खिड़कियाँ, दरवाज़े आदि बनवाने में इनका उपयोग करते हैं।
रथयात्रा एक सामुदायिक पर्व है। घरों में कोई भी पूजा इस अवसर पर नहीं होती है तथा न ही कोई उपवास रखा जाता है। जगन्नाथपुरी और भगवान जगन्नाथ की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। यहां किसी प्रकार का जातिभेद नहीं है। जगन्नाथ के लिए पकाया गया चावल वहां के पुरोहित निम्न कोटि के नाम से पुकारे जाने वाले लोगों से भी लेते हैं। जगन्नाथ को चढ़ाया हुआ चावल कभी अशुद्घ नहीं होता, इसे 'महाप्रसाद' की संज्ञा दी गयी है। इसकी विशेषता रथयात्रा पर्व की महत्ता है। इसका पुरी के चौबीस पर्वों में सर्वाधिक महत्व है। रथ तीर्थ यात्रियों और कुशल मजदूरों द्वारा खींचे जाते हैं। भावुकतापूर्ण गीतों से यह 'महा उत्सव' मनाया जाता है।
जगन्नाथ रथयात्रा, उड़ीसा
अधिक मास में उत्सव
जिस वर्ष आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, उस वर्ष रथयात्रा - उत्सव के साथ एक नया महोत्सव और भी होता है, जिसे 'नवकलेवर उत्सव' कहते हैं। इस उत्सव पर भगवान जगन्नाथ अपना पुराना कलेवर त्याग कर नया कलेवर धारण करते हैं, अर्थात लकड़ियों की नयी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तथा पुरानी मूर्तियों को मन्दिर परिसर में ही 'कोयली वैकुण्ठ' नामक स्थान पर भू - समाधि दे दी जाती है।
Subscribe to:
Comments (Atom)